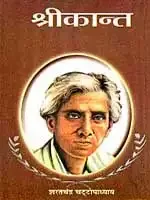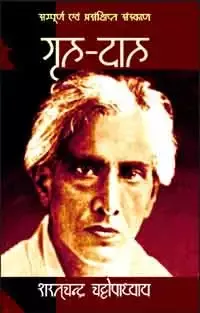|
बहुभागीय पुस्तकें >> श्रीकान्त - भाग 2 श्रीकान्त - भाग 2शरत चन्द्र चट्टोपाध्याय
|
154 पाठक हैं |
||||||
श्रीकान्त का दूसरा भाग...
इस पुस्तक का सेट खरीदें।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
श्रीकान्त-2
एक
जिस भ्रमण-कथा के बीच ही में अचानक एक दिन यवनिका खींचकर विदा हुआ था, कभी
फिर उसी को अपने हाथ से उद्घाटित करने की अपनी प्रवृत्ति न थी।
मेरे
गाँव के रिश्ते के दादाजी-वे जब मेरी नाटकीय उक्ति के जवाब में सिर्फ जरा
मुस्कराए तथा राजलक्ष्मी के झुककर प्रणाम करते जाने पर जिस ढंग से
हड़बड़ाकर दो कदम हट गए और बोले- ‘अच्छा ! अहा, ठीक तो है !
बहुत
अच्छा ! जीते-जागते रहो !’ कहते हुए कौतूहल के साथ डाक्टर को
साथ
लेकर निकल गए, तो उस समय राजलक्ष्मी के चेहरे की जो दशा देखी, वह भूलने की
नहीं, भूला भी नहीं; लेकिन यह सोचा था कि वह नितान्त मेरी ही है- दुनिया
पर वह कभी किसी रूप में जाहिर न हो- परन्तु अब लगता है, अच्छा ही हुआ बहुत
दिनों के बन्द दरवाजे को फिर मुझी को आकर खोलना पड़ा। जिस अनजान रहस्य के
लिए बाहर का क्रोधित संशय अविचार का रूप धारण करके बार-बार धक्के मार रहा
है, यह अच्छा ही हुआ कि बन्द द्वार का अर्गल खोलने का मुझे ही मौका मिला।
दादाजी चले गए। राजलक्ष्मी ज़रा देर ठक्-सी उनकी ओर देखती रही, फिर नजर उठाकर हँसने की बेकार कोशिश करके बोली, ‘पैरों की धूल लेने गई थी, छू नहीं देती उनको। मगर तुम ऐसा क्यों बोल बैठे ? इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी ! यह सिर्फ....’
वास्तव में यह तो सिर्फ अपने लोगों का अपमान किया इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाजार की बाई जी से विधवा-विवाह की पत्नी इनके सामने ऊँचा स्थान नहीं पा सकती- लिहाजा मैं नीचे ही उतरा, किसी को भी जरा-सा ऊपर नहीं उठा सका, राजलक्ष्मी वही कहने जा रही थी, पूरा नहीं कर सकी।
अब समझा। उस अवमानिता के आगे लम्बी हाँककर बात बढ़ाने की इच्छा न हुई। जिस प्रकार से चुप पड़ा था, उसी प्रकार लेटा रहा।
बड़ी देर तक राजलक्ष्मी भी एक शब्द न बोली, मानों अपनी चिन्ता में डूबी बैठी रही। उसके बाद एकाएक करीब कहीं पुकार सुनकर वह मानों चौंकर खड़ी हो गई। रतन को पुकारकर कहा, ‘रतन, कह दे गाड़ी जल्द तैयार करे, नहीं तो फिर रात को ग्यारह बजे वाली गाड़ी से जाना पड़ेगा। और वह हर्गिज अच्छा न होगा, बड़ी सर्दी लगेगी।’
दस ही मिनट के अन्दर रतन ने मेरा बैग उठाकर गाड़ी पर रख दिया और बिस्तर मोड़ने का इशारा करके मेरे पास खड़ा हो गया। तब से मैंने एक भी शब्द न कहा था, अभी भी न बोला। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी बिना पूछे चुपचाप जाकर गाड़ी पर सवार हो गया। कई दिन पहले ऐसी ही एक साँझ को अपने घर आया था, आज फिर वैसी ही साँझ की बेला में घर से चुपचाप निकल पड़ा। उस रोज भी किसी ने आदर से नहीं अपनाया था, आज भी कोई स्नेह के साथ विदा करने के लिए आगे नहीं आया। उस रोज भी उस समय घर-घर में शंख बजना शुरू हुआ था, वसु-मल्लिक के गोपाल-मन्दिर से आरती के घण्टा-घड़ियाल की आवाज हवा में तिरती हुई आ रही थी। मगर उस दिन से आज का कितना अन्तर था, इसे केवल आकाश के देवता ही देखने लगे।
बंगाल के इस मामूली गाँव के टूटे-फूटे के प्रति ममता मुझे कभी भी न थी और इससे पहले इस वंचित होने को भी मैंने कभी हानिकारक नहीं माना, लेकिन आज जब नितान्त अनादर में ही गाँव को छोड़कर चला, कभी किसी बहाने फिर यहाँ कदम रखने कल्पना तक को भी जब मन में जगह न दे सका, तभी यह अस्वास्थ्यकर मामूली-सा गाँव सभी प्रकार से मेरी आँखों के सामने असमान्य होकर प्रकट हुआ। और, जिस घर में अभी-अभी निर्वासित होकर निकला, अपने बाप-दादे के उस टूटे-फूटे पुराने मकान पर मेरे लोभ की आज कोई सीमा नहीं रही।
राजलक्ष्मी चुपचाप आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई और शायद किसी पहचाने पथिक के कौतूहल से अपने को सर्वथा बचाने के ख्याल से ही गाड़ी के एक कोने में सिर रखकर उसने आँखे बन्द कर लीं।
स्टेशन के लिए जब रवाना हुआ, उसके बहुत पहले ही सूर्यदेव डूब चुके थे। गाँव की आँकी-फाँकी डगर के दोनों किनारे मनमाने बढ़े हुए बैंची, झर-बेरी तथा बेर की झाड़ियों ने संकरे रास्ते को और भी संकरा कर दिया था। माझे के ऊपर आम-कटहल की घनी शाखाओं ने मिलकर जगह-जगह पर साँझ के अंधेरे को दुर्भेद बना दिया था। इसके बीच से गाड़ी जब बड़ी सावधानी और धीमी चाल से चलने लगी तो दोनों आँखें खोलकर मैं उस गहरे अँधेरे में मानो कितना क्या देखने लगा। जी में आया, एक दिन इसी राह से मेरे दादा मेरी दादी को ब्याह कर लाए थे, उस रोज यही रास्ता बरातियों की चहल-पहल और पैरों से मुखरित हो उठा था। और फिर जिस दिन वे स्वर्ग सिधारे, तो पड़ोसी लोग इसी रास्ते से उनके शव को ढोकर नदी ले गए थे। इसी रास्ते से होकर एक दिन मेरी माँ-बहू बनकर इस घर में आई थीं और फिर जिस दिन उनके जीवन का अन्त हुआ, तो धूल-गर्द वाले इसी रास्ते से हम लोग उन्हें माँ-गंगा की गोद में रख आए थे। उस समय तक भी यह रास्ता इतना सूना और ऐसा दुर्गम नहीं उठा था, तब भी शायद इसकी हवा में इतना मलेरिया, पोखरों में इतनी कीच और जहर नहीं भर उठा था।
तभी भी देश में अन्न था, वस्त्र था, धर्म था- देश का निरानन्द इतना खौफनाक होकर आसमान को छापते हुए भगवान के द्वार तक धक्का मारने को नहीं जा धमका था। दोनों आँखें भर आईं- गाड़ी के पहिए से थोड़ी-सी धूल लेकर चेहरे और माथे पर लगाते हुए मन-ही-मन बोल उठा, ‘मेरे बाप-दादे के सुख-दु:ख, आपद-विपद, हँसी-रुदन से सने ऐ मेरे धूल-बालू भरे रास्ते, तुम्हें बार-बार प्रणाम।’ उस अँधेरे में वन की ओर देखते हुए कहा, ‘ऐ मेरी जन्म भूमि माँ, तुम्हारी दूसरी करोड़ों अकृति सन्तान की नाईं मैंने भी कभी तुम्हें प्यार नहीं किया। तुम्हारी सेवा, तुम्हारे काम के लिए तुम्हारे पास कभी लौटकर आऊँगा भी या नहीं, नहीं जानता, लेकिन निर्वासन की इस घड़ी में आज धेरी डगर पर तुम्हारे दु:ख की जो मूर्ति मेरे आँसुओं के बीच से धुँधली-सी फूट उठी, उसे मैं जीवन में कभी नहीं भूलूँगा।’
देखा, राजलक्ष्मी वैसी स्थिर बैठी है। अंधेरे में उसकी शक्ल दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन ऐसा लगा, आँखें बन्द किए हुए चिन्ता में डूब गई है। मन-ही-मन बोला, ‘खैर। अपनी फिक्र की नैया की पतवार आज से जब उसी के हाथ छोड़ दी है, तो इस अनजानी नदी में कहाँ भँवर है, कहाँ चोर है- इसे वही ढूँढू निकाले।
जीवन में मैंने अपने मन को विभिन्न प्रकार से, अनेक परिस्थितियों में परख कर देखा है। इनकी नब्ज मैं पहचानता हूँ। इसे बहुत अधिक कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। बहुत ज्यादा सुख, बहुत ज्यादा तन्दरुस्ती आराम से रहना इसे सदा खलता है। यह जानते ही की कोई बहुत ही प्यार करती है- जो मन भाग-भाग करता रहता है, उस मन में कितने बड़े दु:ख से पतवार डाल दी है, इसे मन के बनाने वाले के सिवाय और कौन जाने !
एक बार बाहर के काले आसमान की ओर निगाह फैलाई, अन्दर अदृश्य-सी उस निश्चल प्रतिमा की ओर भी ताका, उसके बाद कह नहीं सकता हाथ जोड़कर किसे नमस्कार किया; लेकिन अपने तईं कहा, ‘इसके आकर्षण के दुस्सह वेग ने मेरी साँस को जैसे रोक डाला है- बहुत बार भागा फिरा मैं, बहुतेरे रास्तों से भागा, मगर गोरख-धन्धे की तरह रास्ते ने जब बार-बार मुझे इसी के हाथों पहुँचाया, तो अब विद्रोह न करूँगा, अब सब प्रकार से अपने को इसी के हाथों सौंप दिया। जीवन की पतवार को अपने ही हाथों रखकर क्या पाया ? इसे कितना सार्थक कर पाया ? फिर अगर यह ऐसे ही एक हाथ में पड़ जाए, जिस सिर से पाँव तक कीच में डूबे हुए अपने जीवन को उठाया है, तो वह दूसरे एक जीवन को हर्गिज उसी में गर्क नहीं करेगी।’
लेकिन यह तो मेरी तरफ की बात हुई- दूसरे पक्ष का फिर वही पुराना रवैया शुरू हुआ। रस्तेभर कोई बात नहीं हुई, यहाँ तक कि स्टेशन पहुँचकर भी किसी ने मुझसे कुछ पूछने-पाछने की जरूरत नहीं समझी। कुछ ही देर कलकत्ते वाली गाड़ी की घण्टी बजी। लेकिन टिकट खरीदना छोड़कर रतन मुसाफिरखाने के एक कोने में मेरा बिस्तर लगने लगा। यह समझ में आया कि इधर जाना न होगा, सुबह की गाड़ी से पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा। पटना या काशी या और कहीं, यह तो नहीं जाना जा सका फिर भी यह खूब समझ में आया कि इसके बारे में राय बिल्कुल बेकार है।
राजलक्ष्मी दूसरी तरफ ताकती हुई अनमनी-सी खड़ी थी। रतन जिस काम में लगा था, उसे पूरा करके आया और बोला, ‘माँ जी, पता चला, जरा पहले जाया जाए तो जो चाहिए, वही भोजन उम्दा मिल जाएगा।’
राजलक्ष्मी ने आँचल की गाँठ से रुपये निकालकर उसे देते हुए कहा, ‘ठीक तो है, जा। मगर दूध जरा समझ-बूझकर लेना, बासी-वासी मत उठा लाना।’
रतन ने पूछा, ‘माँ जी, कुछ आपके लिए....’
‘नहीं, मेरे लिए नहीं लाना है।’
उसके लिए ‘नहीं’ को हम सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा शायद खुद रतन जानता है। फिर भी उसने दो-एक बार-पाँव रगड़कर धीरे-धीरे कहा, ‘कल ही से तो करीब-करीब......’
जवाब में राजलक्ष्मी ने कहा, ‘तू क्या सुन नहीं पाता रतन ? बहरा हो गया है ?’
रतन ने और कुछ नहीं कहा। इसके बाद भी दलील दे, ऐसा जोरदार पक्ष भी है कोई, मुझे पता नहीं। और फिर ज़रूरत भी क्या ? राजलक्ष्मी अपनी जबान से कबूल करे या नहीं, मुझे मालूम है कि रेलगाड़ी में या रास्ते में किसी के हाथ का कुछ खाने की उसे रुचि नहीं। अगर यह कहूँ कि नाहक ही कठिन उपवास करने में इसका सानी नहीं, तो अत्युक्ति न होगी। जाने कितनी बार इसके यहाँ कितनी चीजें मैंने आते देखी हैं, दास-दासियों ने खाईं, पड़ोसी के यहाँ बाँटी गईं, रक्खी-रक्खी खराब हो गईं, फेंक दी गईं, मगर उसने खब मुँह से नहीं लगाया। पूछने पर, मजाक उड़ाने पर कहती, ‘भला, मेरा भी कोई आचार, खाने-छूने का विचार ! मैं सब खाती हूँ।’
‘अच्छा, नजर के सामने मिसाल दो इसकी ?’
‘मिसाल ? अभी ? अरे बाप रे ! फिर बच सकती हूँ भला।’ और न बचने का कोई कारण दिखाए बिना ही वह किसी जरूरी काम के बहाने खिसक पड़ती है। धीरे-धीरे मुझे यह मालूम हो गया था कि वह मछली-मांस, दूध-घी नहीं खाती है, लेकिन यह न खाना उसके लिए इतना अशोभन, इतना शर्मनाक था कि इसका जिक्र करते लाज से वह कहाँ भागे इसके लिए जगह नहीं पाती थी। इसीलिए सहज ही खाने के बारे में अनुरोध करने की इच्छा नहीं होती थी। रतन उदास मुँह लिए चला गया, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में लोटे में गर्म दूध और थोड़ी-सी मिठाई वगैरह लेकर लौटा तो राजलक्ष्मी ने मेरे लिए दूध और थोड़ी-सी मिठाई रखकर बाकी उसी को दे दिया। मैंने कुछ नहीं कहा और रतन की नीरव आँखों की करुण विनती को साफ समझने पर भी मौन रहा।
दादाजी चले गए। राजलक्ष्मी ज़रा देर ठक्-सी उनकी ओर देखती रही, फिर नजर उठाकर हँसने की बेकार कोशिश करके बोली, ‘पैरों की धूल लेने गई थी, छू नहीं देती उनको। मगर तुम ऐसा क्यों बोल बैठे ? इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी ! यह सिर्फ....’
वास्तव में यह तो सिर्फ अपने लोगों का अपमान किया इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाजार की बाई जी से विधवा-विवाह की पत्नी इनके सामने ऊँचा स्थान नहीं पा सकती- लिहाजा मैं नीचे ही उतरा, किसी को भी जरा-सा ऊपर नहीं उठा सका, राजलक्ष्मी वही कहने जा रही थी, पूरा नहीं कर सकी।
अब समझा। उस अवमानिता के आगे लम्बी हाँककर बात बढ़ाने की इच्छा न हुई। जिस प्रकार से चुप पड़ा था, उसी प्रकार लेटा रहा।
बड़ी देर तक राजलक्ष्मी भी एक शब्द न बोली, मानों अपनी चिन्ता में डूबी बैठी रही। उसके बाद एकाएक करीब कहीं पुकार सुनकर वह मानों चौंकर खड़ी हो गई। रतन को पुकारकर कहा, ‘रतन, कह दे गाड़ी जल्द तैयार करे, नहीं तो फिर रात को ग्यारह बजे वाली गाड़ी से जाना पड़ेगा। और वह हर्गिज अच्छा न होगा, बड़ी सर्दी लगेगी।’
दस ही मिनट के अन्दर रतन ने मेरा बैग उठाकर गाड़ी पर रख दिया और बिस्तर मोड़ने का इशारा करके मेरे पास खड़ा हो गया। तब से मैंने एक भी शब्द न कहा था, अभी भी न बोला। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी बिना पूछे चुपचाप जाकर गाड़ी पर सवार हो गया। कई दिन पहले ऐसी ही एक साँझ को अपने घर आया था, आज फिर वैसी ही साँझ की बेला में घर से चुपचाप निकल पड़ा। उस रोज भी किसी ने आदर से नहीं अपनाया था, आज भी कोई स्नेह के साथ विदा करने के लिए आगे नहीं आया। उस रोज भी उस समय घर-घर में शंख बजना शुरू हुआ था, वसु-मल्लिक के गोपाल-मन्दिर से आरती के घण्टा-घड़ियाल की आवाज हवा में तिरती हुई आ रही थी। मगर उस दिन से आज का कितना अन्तर था, इसे केवल आकाश के देवता ही देखने लगे।
बंगाल के इस मामूली गाँव के टूटे-फूटे के प्रति ममता मुझे कभी भी न थी और इससे पहले इस वंचित होने को भी मैंने कभी हानिकारक नहीं माना, लेकिन आज जब नितान्त अनादर में ही गाँव को छोड़कर चला, कभी किसी बहाने फिर यहाँ कदम रखने कल्पना तक को भी जब मन में जगह न दे सका, तभी यह अस्वास्थ्यकर मामूली-सा गाँव सभी प्रकार से मेरी आँखों के सामने असमान्य होकर प्रकट हुआ। और, जिस घर में अभी-अभी निर्वासित होकर निकला, अपने बाप-दादे के उस टूटे-फूटे पुराने मकान पर मेरे लोभ की आज कोई सीमा नहीं रही।
राजलक्ष्मी चुपचाप आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई और शायद किसी पहचाने पथिक के कौतूहल से अपने को सर्वथा बचाने के ख्याल से ही गाड़ी के एक कोने में सिर रखकर उसने आँखे बन्द कर लीं।
स्टेशन के लिए जब रवाना हुआ, उसके बहुत पहले ही सूर्यदेव डूब चुके थे। गाँव की आँकी-फाँकी डगर के दोनों किनारे मनमाने बढ़े हुए बैंची, झर-बेरी तथा बेर की झाड़ियों ने संकरे रास्ते को और भी संकरा कर दिया था। माझे के ऊपर आम-कटहल की घनी शाखाओं ने मिलकर जगह-जगह पर साँझ के अंधेरे को दुर्भेद बना दिया था। इसके बीच से गाड़ी जब बड़ी सावधानी और धीमी चाल से चलने लगी तो दोनों आँखें खोलकर मैं उस गहरे अँधेरे में मानो कितना क्या देखने लगा। जी में आया, एक दिन इसी राह से मेरे दादा मेरी दादी को ब्याह कर लाए थे, उस रोज यही रास्ता बरातियों की चहल-पहल और पैरों से मुखरित हो उठा था। और फिर जिस दिन वे स्वर्ग सिधारे, तो पड़ोसी लोग इसी रास्ते से उनके शव को ढोकर नदी ले गए थे। इसी रास्ते से होकर एक दिन मेरी माँ-बहू बनकर इस घर में आई थीं और फिर जिस दिन उनके जीवन का अन्त हुआ, तो धूल-गर्द वाले इसी रास्ते से हम लोग उन्हें माँ-गंगा की गोद में रख आए थे। उस समय तक भी यह रास्ता इतना सूना और ऐसा दुर्गम नहीं उठा था, तब भी शायद इसकी हवा में इतना मलेरिया, पोखरों में इतनी कीच और जहर नहीं भर उठा था।
तभी भी देश में अन्न था, वस्त्र था, धर्म था- देश का निरानन्द इतना खौफनाक होकर आसमान को छापते हुए भगवान के द्वार तक धक्का मारने को नहीं जा धमका था। दोनों आँखें भर आईं- गाड़ी के पहिए से थोड़ी-सी धूल लेकर चेहरे और माथे पर लगाते हुए मन-ही-मन बोल उठा, ‘मेरे बाप-दादे के सुख-दु:ख, आपद-विपद, हँसी-रुदन से सने ऐ मेरे धूल-बालू भरे रास्ते, तुम्हें बार-बार प्रणाम।’ उस अँधेरे में वन की ओर देखते हुए कहा, ‘ऐ मेरी जन्म भूमि माँ, तुम्हारी दूसरी करोड़ों अकृति सन्तान की नाईं मैंने भी कभी तुम्हें प्यार नहीं किया। तुम्हारी सेवा, तुम्हारे काम के लिए तुम्हारे पास कभी लौटकर आऊँगा भी या नहीं, नहीं जानता, लेकिन निर्वासन की इस घड़ी में आज धेरी डगर पर तुम्हारे दु:ख की जो मूर्ति मेरे आँसुओं के बीच से धुँधली-सी फूट उठी, उसे मैं जीवन में कभी नहीं भूलूँगा।’
देखा, राजलक्ष्मी वैसी स्थिर बैठी है। अंधेरे में उसकी शक्ल दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन ऐसा लगा, आँखें बन्द किए हुए चिन्ता में डूब गई है। मन-ही-मन बोला, ‘खैर। अपनी फिक्र की नैया की पतवार आज से जब उसी के हाथ छोड़ दी है, तो इस अनजानी नदी में कहाँ भँवर है, कहाँ चोर है- इसे वही ढूँढू निकाले।
जीवन में मैंने अपने मन को विभिन्न प्रकार से, अनेक परिस्थितियों में परख कर देखा है। इनकी नब्ज मैं पहचानता हूँ। इसे बहुत अधिक कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। बहुत ज्यादा सुख, बहुत ज्यादा तन्दरुस्ती आराम से रहना इसे सदा खलता है। यह जानते ही की कोई बहुत ही प्यार करती है- जो मन भाग-भाग करता रहता है, उस मन में कितने बड़े दु:ख से पतवार डाल दी है, इसे मन के बनाने वाले के सिवाय और कौन जाने !
एक बार बाहर के काले आसमान की ओर निगाह फैलाई, अन्दर अदृश्य-सी उस निश्चल प्रतिमा की ओर भी ताका, उसके बाद कह नहीं सकता हाथ जोड़कर किसे नमस्कार किया; लेकिन अपने तईं कहा, ‘इसके आकर्षण के दुस्सह वेग ने मेरी साँस को जैसे रोक डाला है- बहुत बार भागा फिरा मैं, बहुतेरे रास्तों से भागा, मगर गोरख-धन्धे की तरह रास्ते ने जब बार-बार मुझे इसी के हाथों पहुँचाया, तो अब विद्रोह न करूँगा, अब सब प्रकार से अपने को इसी के हाथों सौंप दिया। जीवन की पतवार को अपने ही हाथों रखकर क्या पाया ? इसे कितना सार्थक कर पाया ? फिर अगर यह ऐसे ही एक हाथ में पड़ जाए, जिस सिर से पाँव तक कीच में डूबे हुए अपने जीवन को उठाया है, तो वह दूसरे एक जीवन को हर्गिज उसी में गर्क नहीं करेगी।’
लेकिन यह तो मेरी तरफ की बात हुई- दूसरे पक्ष का फिर वही पुराना रवैया शुरू हुआ। रस्तेभर कोई बात नहीं हुई, यहाँ तक कि स्टेशन पहुँचकर भी किसी ने मुझसे कुछ पूछने-पाछने की जरूरत नहीं समझी। कुछ ही देर कलकत्ते वाली गाड़ी की घण्टी बजी। लेकिन टिकट खरीदना छोड़कर रतन मुसाफिरखाने के एक कोने में मेरा बिस्तर लगने लगा। यह समझ में आया कि इधर जाना न होगा, सुबह की गाड़ी से पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा। पटना या काशी या और कहीं, यह तो नहीं जाना जा सका फिर भी यह खूब समझ में आया कि इसके बारे में राय बिल्कुल बेकार है।
राजलक्ष्मी दूसरी तरफ ताकती हुई अनमनी-सी खड़ी थी। रतन जिस काम में लगा था, उसे पूरा करके आया और बोला, ‘माँ जी, पता चला, जरा पहले जाया जाए तो जो चाहिए, वही भोजन उम्दा मिल जाएगा।’
राजलक्ष्मी ने आँचल की गाँठ से रुपये निकालकर उसे देते हुए कहा, ‘ठीक तो है, जा। मगर दूध जरा समझ-बूझकर लेना, बासी-वासी मत उठा लाना।’
रतन ने पूछा, ‘माँ जी, कुछ आपके लिए....’
‘नहीं, मेरे लिए नहीं लाना है।’
उसके लिए ‘नहीं’ को हम सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा शायद खुद रतन जानता है। फिर भी उसने दो-एक बार-पाँव रगड़कर धीरे-धीरे कहा, ‘कल ही से तो करीब-करीब......’
जवाब में राजलक्ष्मी ने कहा, ‘तू क्या सुन नहीं पाता रतन ? बहरा हो गया है ?’
रतन ने और कुछ नहीं कहा। इसके बाद भी दलील दे, ऐसा जोरदार पक्ष भी है कोई, मुझे पता नहीं। और फिर ज़रूरत भी क्या ? राजलक्ष्मी अपनी जबान से कबूल करे या नहीं, मुझे मालूम है कि रेलगाड़ी में या रास्ते में किसी के हाथ का कुछ खाने की उसे रुचि नहीं। अगर यह कहूँ कि नाहक ही कठिन उपवास करने में इसका सानी नहीं, तो अत्युक्ति न होगी। जाने कितनी बार इसके यहाँ कितनी चीजें मैंने आते देखी हैं, दास-दासियों ने खाईं, पड़ोसी के यहाँ बाँटी गईं, रक्खी-रक्खी खराब हो गईं, फेंक दी गईं, मगर उसने खब मुँह से नहीं लगाया। पूछने पर, मजाक उड़ाने पर कहती, ‘भला, मेरा भी कोई आचार, खाने-छूने का विचार ! मैं सब खाती हूँ।’
‘अच्छा, नजर के सामने मिसाल दो इसकी ?’
‘मिसाल ? अभी ? अरे बाप रे ! फिर बच सकती हूँ भला।’ और न बचने का कोई कारण दिखाए बिना ही वह किसी जरूरी काम के बहाने खिसक पड़ती है। धीरे-धीरे मुझे यह मालूम हो गया था कि वह मछली-मांस, दूध-घी नहीं खाती है, लेकिन यह न खाना उसके लिए इतना अशोभन, इतना शर्मनाक था कि इसका जिक्र करते लाज से वह कहाँ भागे इसके लिए जगह नहीं पाती थी। इसीलिए सहज ही खाने के बारे में अनुरोध करने की इच्छा नहीं होती थी। रतन उदास मुँह लिए चला गया, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में लोटे में गर्म दूध और थोड़ी-सी मिठाई वगैरह लेकर लौटा तो राजलक्ष्मी ने मेरे लिए दूध और थोड़ी-सी मिठाई रखकर बाकी उसी को दे दिया। मैंने कुछ नहीं कहा और रतन की नीरव आँखों की करुण विनती को साफ समझने पर भी मौन रहा।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book